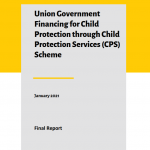दूरस्थ शिक्षण: एक अवसर या चुनौती?
8 May 2020
जैसे–जैसे COVID-19 ने अपने पैर पसारे, वैसे–वैसे शिक्षण संस्थानों के दरवाज़े बंद होते चले गए। आज स्थिति ये है कि, COVID-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए दुनिया भर की अधिकांश सरकारों ने शिक्षण संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। और शिक्षा के इस राष्ट्रव्यापी बंद के कारण छात्र आबादी प्रभावित हो रही है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है की- क्या कोरोनावायरस दूरस्थ शिक्षण के लिए एक अवसर है? और क्या इससे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा?
एक तरफ जहां ऐसे समय में अधिकांश देश, शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने के लिए डिजिटल रूप से दूरस्थ शिक्षा का उपयोग कर रहे है। वहीँ दूसरी तरफ चुनौती ये है कि, दुनिया भर में 50 प्रतिशत (826 मिलियन) छात्रों के पास घरेलू कंप्यूटर नहीं है और 43 प्रतिशत (706 मिलियन) के पास घर पर इंटरनेट नहीं है।
ऐसे में जब हम भारत की स्थिति पर गौर करें तो, जनवरी 2020 तक देश की डिजिटल आबादी लगभग 688 मिलियन सक्रिय हो गई थी। COVID-19 संकट से पहले भी भारत में डिजिटल शिक्षा को महत्त्व दिया जा रहा था। KPMG और Google के अध्ययन अनुसार, भारत में ऑनलाइन शिक्षा बाजार, 2021 तक 9.6 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ 1.96 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान था। साथ ही, भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी (edtech) कंपनी बायजू, मार्च 2019 में, दुनिया की सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनी थी। और यह भारत के छोटे शहरों और कस्बों में भी निरंतर अपनी पहचान बना रही थी।
उपरोक्त आंकड़ों के हिसाब से भारत के लिए दूरस्थ शिक्षण पद्धति एक अवसर के रूप में भविष्य के लिए कारगर साबित हो सकती है। लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि क्या हमारे शिक्षक इसके लिए तैयार है? शिक्षकों को भी दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित ऐसे रूझानों का अनुसरण करें तो:
शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षण पद्धतियों में बदलाव की गति बहुत धीमी रही है। COVID-19 अपेक्षाकृत कम समय में अभिनव समाधानों की खोज के लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए उत्प्रेरक बन गया है। भारत में बिहार में शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से दूरदर्शन के DD बिहार चैनल पर “मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय” कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को पाठ्य-पुस्तक आधारित शिक्षण लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में सरकार पहली कक्षा से कॉलेज विद्यार्थियों के लिए इ-लर्निंग कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए WhatsApp के ज़रिये सभी विषयों के टेस्ट-पेपर आयोजित करवाए जा रहे है।
ऐसा हो सकता है की शिक्षण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़े। पिछले कुछ हफ्तों में, हमने विभिन्न हितधारकों के साथ-साथ सरकारों, प्रकाशकों, शिक्षा पेशेवरों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, और दूरसंचार नेटवर्क ऑपरेटरों के गठबंधन को आकार लेते हुए देखा है, जो संकट के अस्थायी समाधान के रूप में डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। विकासशील देशों में जहां शिक्षा मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई है, यह भविष्य की शिक्षा के लिए एक प्रचलित और परिणामी प्रवृत्ति बन सकती है।
आखिर में प्रभावित क्षेत्रों के अधिकांश स्कूलों में शिक्षण जारी रखने के लिए स्टॉप-गैप (सामयिक उपाय) समाधान मिल रहे हैं। लेकिन सीखने की गुणवत्ता, डिजिटल पहुंच के स्तर और डिजिटल गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जब तक डिजिटल पहुंच की लागत और डिजिटल गुणवत्ता में वृद्धि नहीं होती है, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ सकता है।
अगले ब्लॉग में मेरे सहयोगी इन अवसरों और उसके चलते चुनौतियों में से कुछ पर ध्यान केन्द्रित करेंगे बिहार के संदर्भ में।
पूनम Accountability Initiative में सीनियर पैसा एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं।